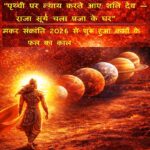सात साल पहले मंदसौर में 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म ने पूरे समाज को झकझोर दिया था। सेशन न्यायालय और बाद में हाई कोर्ट ने आजाद भारत में पहली बार जिले के दो आरोपियों को फांसी की सज़ा दी थी। किंतु हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के दखल ने इस सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया। इसके विरोध में मंदसौर शहर बंद रखा गया, प्रदर्शन हुए और एक बार फिर ‘फांसी की सज़ा’ राष्ट्रीय बहस में लौट आई।
प्रश्न यह है कि क्या जनआक्रोश न्यायिक निर्णयों को बदलवा सकता है? क्या किसी मंत्री, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि को यह अधिकार है कि वह अदालत के फैसले को पलट सके? लोकतंत्र में जनता को अपनी राय रखने का अधिकार है, परंतु अंतिम निर्णय संविधान और कानून के अधीन न्यायपालिका ही करती है — वह भी साक्ष्य, विधिक सिद्धांतों और प्रक्रिया के तहत।
“दुर्लभतम से दुर्लभ” सिद्धांत और न्यायिक विवेक
भारत में फांसी की सज़ा केवल “दुर्लभतम से दुर्लभ” (Rarest of Rare) मामलों में दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसमें अपराध की प्रकृति के साथ-साथ अपराधी की मानसिकता, सामाजिक पृष्ठभूमि, सुधार की संभावना आदि को देखा जाता है।
निर्भया कांड (2012) इसका उदाहरण है, जिसमें सज़ा क्रूरता, पुख्ता साक्ष्य और दुर्लभतम प्रकृति के आधार पर दी गई। वहीं कठुआ बलात्कार (2018) में व्यापक जनाक्रोश के बावजूद कोर्ट ने आजीवन कारावास को पर्याप्त माना, क्योंकि वह ‘दुर्लभतम’ श्रेणी में नहीं आता था।
जस्टिस दीपक मिश्रा का एक कथन उल्लेखनीय है कि — “जनता की भावना महत्वपूर्ण है, लेकिन न्याय भीड़ से नहीं, बल्कि संविधान और कानून से होता है।”
लोक अभियोजन की भूमिका पर भी सवाल
मंदसौर केस में भी यह सवाल उठ रहा है कि जब शहर के वकीलों ने आरोपियों की पैरवी से इनकार किया, माना गया कि आरोपियों की हैसियत वकील नियुक्त करने की नहीं है,तब बाहर से वकील कैसे आए? और क्यों आए?
साथ ही, यह भी कि सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट को पर्याप्त न मानते हुए वैज्ञानिक विशेषज्ञ के बयान को ज़रूरी बताया। क्या यह अभियोजन पक्ष की कमजोर रणनीति या साक्ष्य प्रस्तुति की चूक नहीं थी?
यह तथ्य भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि फांसी की सज़ा कम होने पर जन आक्रोश अभियोजन पक्ष या सरकारी वकीलों की ओर नहीं जाता, जबकि न्यायालय का निर्णय उन्हीं की कार्यशैली पर आधारित होता है। मंदसौर के प्रकरण में अपराधी को मृत्यु पर्यंत जेल में ही रहने की सजा दी गई है।
उल्लेखनीय है कि संविधान में अदालतों के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, जिनके तहत सुनिश्चित करना होता है कि आरोपियों को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिले। यदि उनके लिए कोई वकील उपलब्ध न हो तो अदालत उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करती है।
अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण: फांसी एक नैतिक प्रश्न
दुनिया के 180 देशों में से 110 देशों ने फांसी की सज़ा समाप्त कर दी है। संयुक्त राष्ट्र और मानव अधिकार जैसे संगठनों ने इसे अमानवीय, असमान और अपरिवर्तनीय बताया है।
फांसी का विरोध इसलिए भी होता है क्योंकि न्यायिक भूलें और तकनीकी त्रुटियाँ मानव जीवन को वापस नहीं ला सकतीं। मृत्युदंड के बाद कोई “पुनः न्याय” संभव नहीं।
वहीं समर्थक पक्ष मानता है कि आतंकवाद, बलात्कार और बच्चों के विरुद्ध जघन्य अपराध ऐसे हैं जिनमें कठोरतम सज़ा आवश्यक है। 2020 के एक सर्वेक्षण के अनुसार 70 प्रतिशत भारतीय नागरिक फांसी का समर्थन करते हैं।
न्याय बनाम प्रतिशोध: समाज क्या चाहता है?
क्या न्याय का उद्देश्य बदला लेना है, या सुधार और संतुलन लाना? यदि हर दुष्कर्म के बाद समाज ‘फांसी’ को ही अंतिम न्याय मानेगा, तो यह न्याय की आत्मा के विरुद्ध होगा। यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या हम समान घटनाओं पर समान दृष्टिकोण रखते हैं, या पीड़िता और अपराधियों की धार्मिक पहचान के अनुसार समाज की संवेदना बदलती है?
कुछ तथ्य और आंकड़े:-
भारत में वर्ष 2022 तक 488 मौत की सजाएं सुनाई गईं है।उच्च अदालतों द्वारा इनमें से 99 प्रतिशत मामलों में सज़ा बदली गई।2020 में सिर्फ 4 दोषियों को फांसी दी गई (निर्भया प्रकरण)।सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई फांसी की सज़ा दया याचिका के बाद कई बार आजीवन कारावास में बदल दी गई है।
मंदसौर की घटना ने यह जरूर दिखाया कि समाज बालिकाओं के प्रति अपराधों को लेकर संवेदनशील है। लेकिन संवेदनशीलता को संविधानिक विवेक से जोड़कर ही सही समाधान निकाला जा सकता है।
जब तक अभियोजन मज़बूत नहीं होगा, साक्ष्य पुख्ता नहीं होंगे और न्याय की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं बनेगी — तब तक सिर्फ ‘फांसी’ की मांग से अपराध नहीं रुकेंगे।